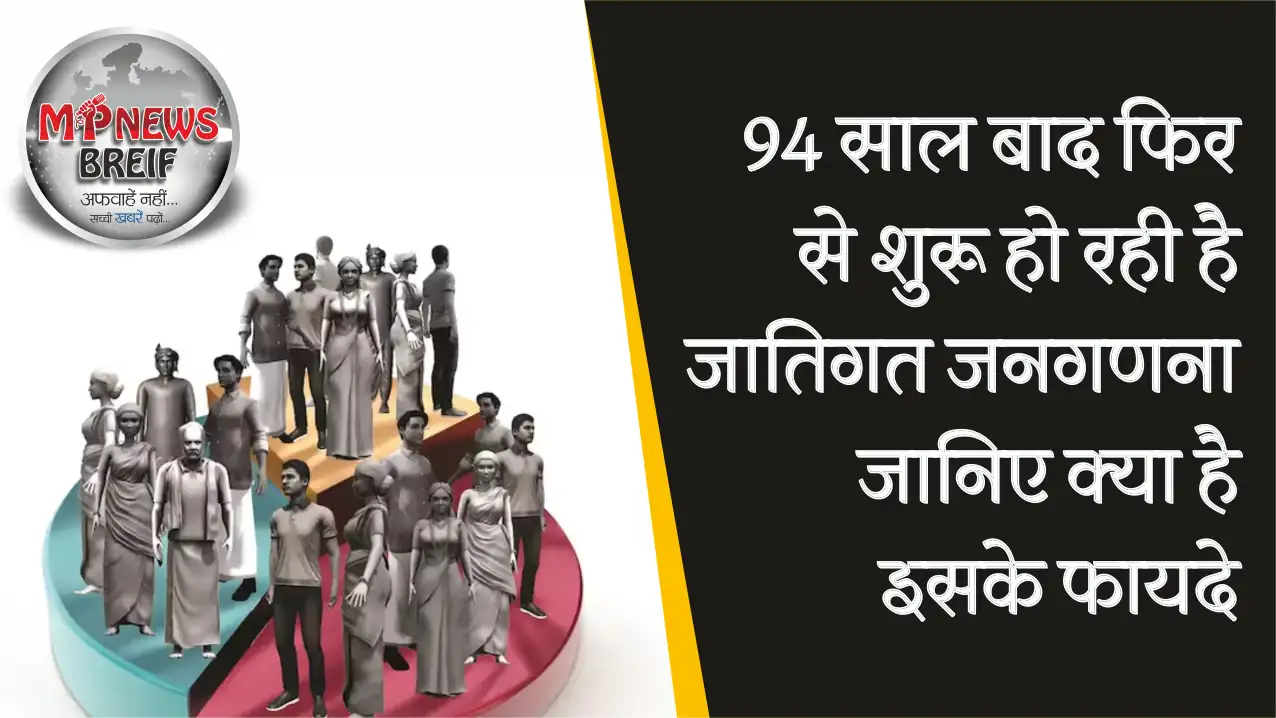94 साल बाद फिर से शुरू हो रही है जातिगत जनगणना जानिए क्या है इसके फायदे
Benefits of Caste Census in India | भारत एक ऐसा देश है, जहाँ जाति व्यवस्था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना का एक अभिन्न हिस्सा रही है। आजादी के बाद से भारत में नियमित रूप से जनगणना तो होती रही है, लेकिन जातिगत जनगणना को लेकर हमेशा से बहस और माँग बनी रही है। आखिरी बार 1931 में ब्रिटिश शासन के दौरान जातिगत जनगणना की गई थी। उसके बाद से यह प्रक्रिया रुक गई थी, और आजादी के बाद की जनगणनाओं में केवल अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और धार्मिक समुदायों की गिनती ही की जाती रही है। लेकिन अब, 94 साल बाद, भारत सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है, जो सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। Benefits of Caste Census in India
17 जून 2025 तक की ताजा जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना की तारीखों का ऐलान कर दिया है। यह प्रक्रिया दो चरणों में होगी, और इसके प्रभाव समाज के हर क्षेत्र पर पड़ने वाले हैं। इस लेख में हम जातिगत जनगणना की शुरुआत, इसकी प्रक्रिया, और इसके संभावित प्रभावों को विस्तार से समझेंगे।
जातिगत जनगणना कब से शुरू होगी?
केंद्र सरकार ने 16 जून 2025 को जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत एक अधिसूचना जारी की, जिसमें जातिगत जनगणना के साथ-साथ राष्ट्रीय जनगणना की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से शुरू करने की घोषणा की गई। यह प्रक्रिया दो चरणों में होगी:
-
पहला चरण: यह 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा और इसमें पहाड़ी और बर्फीले इलाकों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, और जम्मू-कश्मीर को शामिल किया जाएगा। इन क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जनगणना पहले शुरू की जाएगी।
-
दूसरा चरण: यह 1 मार्च 2027 से शुरू होगा और देश के बाकी हिस्सों में जनगणना की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। यह चरण 1 मार्च 2027 को रात 12 बजे तक समाप्त होगा।
इसके साथ ही, यह पहली बार होगा जब भारत में जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी। इसके लिए एक मोबाइल ऐप और जनगणना पोर्टल तैयार किया गया है, और स्व-गणना (Self-Enumeration) का विकल्प भी उपलब्ध होगा। यह प्रक्रिया लगभग 21 महीनों में पूरी होगी, और डेटा को दिसंबर 2027 तक सार्वजनिक करने की उम्मीद है।
यह प्रक्रिया 2021 में होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। अब, 17 साल बाद (2011 की जनगणना के बाद), यह जनगणना न केवल जनसंख्या की गिनती करेगी, बल्कि जातिगत आँकड़े भी जुटाएगी, जो नीति-निर्माण और सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण होंगे।
जातिगत जनगणना की प्रक्रिया
जातिगत जनगणना, राष्ट्रीय जनगणना का हिस्सा होगी और इसे दो मुख्य चरणों में बाँटा गया है:
-
मकान सूचीकरण (हाउसिंग सेंसस): इस चरण में हर परिवार के घर की स्थिति, उपलब्ध सुविधाओं (जैसे पेयजल, शौचालय, बिजली), और संपत्ति से जुड़ी जानकारी जुटाई जाएगी। यह चरण 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा।
-
जनसंख्या गणना (पॉपुलेशन सेंसस): इस चरण में हर व्यक्ति की जनसांख्यिकीय, सामाजिक, और आर्थिक जानकारी एकत्र की जाएगी। इसमें उम्र, लिंग, शिक्षा, रोजगार, प्रवास, और जाति से संबंधित सवाल शामिल होंगे। यह चरण 9 फरवरी 2027 से शुरू होगा और 1 मार्च 2027 तक पूरा होगा।
जातिगत जनगणना के दौरान एक विशेष कॉलम होगा, जिसमें हर व्यक्ति से उनकी जाति और उप-जाति की जानकारी ली जाएगी। इसके लिए 34 लाख कर्मचारी घर-घर जाकर डेटा जुटाएँगे। डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं, ताकि कोई लीक न हो।
जातिगत जनगणना के प्रभाव
जातिगत जनगणना के प्रभाव बहुआयामी होंगे। यह न केवल सामाजिक और आर्थिक नीतियों को प्रभावित करेगी, बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को भी बदल सकती है। आइए, इसके प्रमुख प्रभावों पर नजर डालें:
1. सामाजिक प्रभाव
जातिगत जनगणना से देश में हर जाति की सटीक आबादी का पता चलेगा। इससे सामाजिक असमानताओं को समझने में मदद मिलेगी। खासकर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC), और अनुसूचित जनजाति (ST) की सही संख्या सामने आएगी।
-
शिक्षा और रोजगार में अवसर: जातिगत आँकड़ों के आधार पर सरकार यह समझ सकेगी कि कौन सी जातियाँ शिक्षा और रोजगार के मामले में पीछे हैं। इससे लक्षित योजनाएँ बनाई जा सकेंगी।
-
सामाजिक न्याय: यह जनगणना सामाजिक न्याय को बढ़ावा देगी। जिन जातियों को अब तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है, उन्हें मुख्यधारा में लाने का मौका मिलेगा।
-
जातिगत भेदभाव पर प्रभाव: कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जातिगत आँकड़े सामने आने से जातिगत भेदभाव को कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि सरकार और समाज दोनों को वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। हालांकि, कुछ लोग यह भी तर्क देते हैं कि इससे जातिगत पहचान और मजबूत हो सकती है, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ सकता है।
2. आर्थिक प्रभाव
जातिगत जनगणना से आर्थिक नीतियों पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा।
-
आरक्षण नीतियों में बदलाव: वर्तमान में OBC को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 27% आरक्षण मिलता है, जो 1931 के आँकड़ों पर आधारित है। अगर नए आँकड़े बताते हैं कि OBC की आबादी 52% से ज्यादा है, तो आरक्षण की सीमा बढ़ाने पर विचार हो सकता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 50% आरक्षण की सीमा तय की है, जिसके कारण यह मुद्दा विवादास्पद हो सकता है।
-
संसाधनों का वितरण: केंद्र और राज्य सरकारें जातिगत आँकड़ों के आधार पर संसाधनों का बेहतर वितरण कर सकेंगी। उदाहरण के लिए, जिन जातियों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनके लिए विशेष योजनाएँ बनाई जा सकती हैं।
-
प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण: कुछ लोग माँग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना के बाद प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू किया जाए। यह एक बड़ा आर्थिक बदलाव हो सकता है, लेकिन इसे लागू करना आसान नहीं होगा।
3. राजनीतिक प्रभाव
जातिगत जनगणना का सबसे बड़ा प्रभाव राजनीति पर पड़ेगा।
-
परिसीमन (Delimitation): जनगणना के बाद 2028 में लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन शुरू होगा। जातिगत आँकड़ों के आधार पर यह तय होगा कि किन क्षेत्रों में कौन सी जाति प्रभावशाली है, जिससे राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं।
-
चुनावी रणनीति: राजनीतिक दल जातिगत आँकड़ों का इस्तेमाल अपनी चुनावी रणनीति बनाने में करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर किसी राज्य में OBC की आबादी ज्यादा निकलती है, तो पार्टियाँ उनके लिए विशेष वादे कर सकती हैं।
-
महिला आरक्षण पर असर: 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने की बात चल रही है। लेकिन परिसीमन में देरी होने से यह प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है।
-
जातिगत राजनीति में उछाल: कुछ आलोचकों का मानना है कि जातिगत जनगणना से जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। राजनीतिक दल अपनी सुविधा के अनुसार इन आँकड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ सकता है।
4. डेटा संग्रहण और गोपनीयता
यह जनगणना पहली बार डिजिटल होगी, जिसमें आधार, बायोमेट्रिक, और AI तकनीक का इस्तेमाल होगा। लेकिन इससे डेटा गोपनीयता को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं।
-
सरकार ने डेटा की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम करने का दावा किया है। लेकिन अगर डेटा लीक होता है, तो यह लोगों की निजता पर बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है।
-
डिजिटल जनगणना से प्रक्रिया तेज और सटीक होगी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी जागरूकता की कमी एक चुनौती हो सकती है।
चुनौतियाँ और आलोचनाएँ
जातिगत जनगणना के कई लाभ हैं, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियाँ और आलोचनाएँ भी हैं:
-
जातिगत तनाव का खतरा: कुछ लोग मानते हैं कि जातिगत आँकड़े सामने आने से समाज में बंटवारा बढ़ेगा।
-
डेटा की सटीकता: भारत में जातियों और उप-जातियों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में सटीक डेटा जुटाना एक बड़ी चुनौती होगी।
-
राजनीतिक दुरुपयोग: विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि सरकार इसजनगणना का इस्तेमाल केवल चुनावी लाभ के लिए करेगी।
-
आरक्षण की सीमा: अगर OBC की आबादी ज्यादा निकलती है, तो 50% आरक्षण की सीमा को तोड़ने की माँग बढ़ सकती है, जो कानूनी विवाद का कारण बन सकता है।
जातिगत जनगणना एक ऐतिहासिक कदम है, जो भारत के सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक परिदृश्य को बदल सकता है। यह प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी और 1 मार्च 2027 तक चलेगी। इसके परिणाम दिसंबर 2027 तक सामने आ सकते हैं, जिसके बाद परिसीमन और नई नीतियाँ बनाई जाएँगी। यह जनगणनासामाजिक न्याय को बढ़ावा देगी, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जिन्हें सावधानीपूर्वकसंभालने की जरूरत है। Benefits of Caste Census in India
जातिगत जनगणना से देश में समानता और विकास की नई राह खुल सकती है, लेकिन इसके लिए सरकार को पारदर्शिता और निष्पक्षतासुनिश्चित करनी होगी। यह एक ऐसा कदम है, जो भारत के भविष्य को नई दिशा दे सकता है, बशर्ते इसे सही तरीके से लागू किया जाए। Benefits of Caste Census in India
यह भी पढें…
प्रचंड गर्मी में मोबाइल बन सकता है बम: इन गलतियों से बचें
मैं इंदर सिंह चौधरी वर्ष 2005 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूं। मैंने मास कम्यूनिकेशन में स्नातकोत्तर (M.A.) किया है। वर्ष 2007 से 2012 तक मैं दैनिक भास्कर, उज्जैन में कार्यरत रहा, जहाँ पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया।
वर्ष 2013 से 2023 तक मैंने अपना मीडिया हाउस ‘Hi Media’ संचालित किया, जो उज्जैन में एक विश्वसनीय नाम बना। डिजिटल पत्रकारिता के युग में, मैंने सितंबर 2023 में पुनः दैनिक भास्कर से जुड़ते हुए साथ ही https://mpnewsbrief.com/ नाम से एक न्यूज़ पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से मैं करेंट अफेयर्स, स्वास्थ्य, ज्योतिष, कृषि और धर्म जैसे विषयों पर सामग्री प्रकाशित करता हूं। फ़िलहाल मैं अकेले ही इस पोर्टल का संचालन कर रहा हूं, इसलिए सामग्री सीमित हो सकती है, लेकिन गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होता।